श्रीमद्भगवद्गीता
श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय तीन श्लोक 01-08
कर्मयोग » ज्ञानयोग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण
अर्जुन उवाच
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥
अर्जुनः उवाच – अर्जुन ने कहा; ज्यायसी – श्रेष्ठ; चेत् – यदि; कर्मणः – सकाम कर्म की अपेक्षा; ते – तुम्हारे द्वारा; मता – मानी जाति है; बुद्धिः – बुद्धि; जनार्दन – हे कृष्ण; तत् – अतः; किम् – क्यों फिर; कर्मणि – कर्म में; घोरे – भयंकर, हिंसात्मक; माम् – मुझको; नियोजयसि – नियुक्त करते हो; केशव – हे कृष्ण,
भावार्थ : अर्जुन बोले- हे जनार्दन! यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव! मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं?॥1॥
तात्पर्य : श्रीभगवान् कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ट मित्र अर्जुन को संसार के शोक-सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद् वर्णन किया है और आत्म-साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है – बुद्धियोग या कृष्णभावनामृत । कभी-कभी कृष्णभावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रान्त धारणा वाला मनुष्य भगवान् कृष्ण के नाम-जप द्वारा पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होने के लिए प्रायः एकान्त स्थान में चला जाता है । किन्तु कृष्णभावनामृत-दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकान्त स्थान में कृष्ण नाम-जप करना ठीक नहीं । इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी । अर्जुन को भी कृष्णभावनामृत या बुद्धियोग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकान्त स्थान में तपस्या का अभ्यास हो । दूसरे शब्दों में, वह कृष्णभावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था । किन्तु एकनिष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य-विधि के विषय में प्रश्न किया । उत्तर में भगवान् ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात् कृष्णभावनाभावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी ।
तात्पर्य : श्रीभगवान् कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ट मित्र अर्जुन को संसार के शोक-सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद् वर्णन किया है और आत्म-साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है – बुद्धियोग या कृष्णभावनामृत । कभी-कभी कृष्णभावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रान्त धारणा वाला मनुष्य भगवान् कृष्ण के नाम-जप द्वारा पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होने के लिए प्रायः एकान्त स्थान में चला जाता है । किन्तु कृष्णभावनामृत-दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकान्त स्थान में कृष्ण नाम-जप करना ठीक नहीं । इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी । अर्जुन को भी कृष्णभावनामृत या बुद्धियोग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकान्त स्थान में तपस्या का अभ्यास हो । दूसरे शब्दों में, वह कृष्णभावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था । किन्तु एकनिष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य-विधि के विषय में प्रश्न किया । उत्तर में भगवान् ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात् कृष्णभावनाभावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी ।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥२॥
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥२॥
व्यामिश्रेण – अनेकार्थक; इव – मानो; वाक्येन – शब्दों से; बुद्धिम् – बुद्धि; मोहयसि – मोह रहे हो; इव – मानो; मे – मेरी; तत् – अतः; एकम् – एकमात्र; वाद – कहिये; निश्र्चित्य – निश्चय करके; येन – जिससे; श्रेयः – वास्तविक लाभ; अहम् – मैं; आप्नुयाम् – पा सकूँ,
भावार्थ : आप मिले हुए-से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊँ॥2॥॥
तात्पर्य : पिछले अध्याय में, भगवद्गीता के उपक्रम के रूप मे सांख्ययोग, बुद्धियोग, बुद्धि द्वारा इन्द्रियनिग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है । किन्तु उसमें तारतम्य नहीं था । कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी । अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके । यद्यपि श्रीकृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किन्तु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्णभावनामृत क्या है – जड़ता है या कि सक्रीय सेवा । दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद्गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्णभावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है ।
श्रीभगवानुवाच
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥३॥
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥३॥
श्री-भगवान् उवाच – श्रीभगवान ने कहा; लोके – संसार में; अस्मिन् – इस; द्वि-विधा – दो प्रकार की; निष्ठा – श्रद्धा; पुरा – पहले; प्रोक्ता – कही गई; मया – मेरे द्वारा; अनघ – हे निष्पाप; ज्ञान-योगेन – ज्ञानयोग के द्वारा; सांख्यानाम् – ज्ञानियों का; कर्म-योगेन – भक्तियोग के द्वारा; योगिनाम् – भक्तों का,
भावार्थ : श्रीभगवान बोले- हे निष्पाप! इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा (साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम 'निष्ठा' है।) मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से (माया से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीर द्वारा होने वाली सम्पूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंदघन परमात्मा में एकीभाव से स्थित रहने का नाम 'ज्ञान योग' है, इसी को 'संन्यास', 'सांख्ययोग' आदि नामों से कहा गया है।) और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से (फल और आसक्ति को त्यागकर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम 'निष्काम कर्मयोग' है, इसी को 'समत्वयोग', 'बुद्धियोग', 'कर्मयोग', 'तदर्थकर्म', 'मदर्थकर्म', 'मत्कर्म' आदि नामों से कहा गया है।) होती है॥3॥
तात्पर्य : द्वितीय अध्याय के उन्तालीसवें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है – सांख्ययोग तथा कर्मयोग या बुद्धियोग । इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है । सांख्ययोग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिन्तन एवं मनन करना चाहते हैं । दूसरे प्रकार के लोग कृष्णभावनामृत में कार्य करते हैं जैसा कि द्वितीय अध्याय के इकसठवें श्लोक में बताया गया है । उन्तालीसवें श्लोक में भी भगवान् ने बताया है कि बुद्धियोग या कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बन्धनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है । इकसठवें श्लोक में इसी सिद्धान्त को और अधिक स्पष्ट किया गया है – कि बुद्धियोग पूर्णतया परब्रह्म (विशेषतया कृष्ण) पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इन्द्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है । अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं । दर्शनविहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी-कभी धर्मान्धता है और धर्मविहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है । अन्तिम लक्ष्य तो श्रीकृष्ण हैं क्योंकि जो दार्शनिकजन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अन्ततः कृष्णभावनामृत को प्राप्त होते हैं । इसका भी उल्लेख भगवद्गीता में मिलता है । सम्पूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के सम्बन्ध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है । इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिन्तन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्णभावनामृत तक पहुँचा जा सकता है । प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्णभावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना सम्बन्ध जोड़ना होता है । इन दोनों में से कृष्णभावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इन्द्रियों को विमल नहीं करना होता । कृष्णभावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है ।
न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥४॥
न – नहीं; कर्मणाम् – नियत कर्मों के; अनाराम्भात् – न करने से; नैष्कर्म्यम् – कर्मबन्धन से मुक्ति को; पुरुषः – मनुष्य; अश्नुते – प्राप्त करता है; न – नहीं; च – भी; संन्यसनात् – त्याग से; एव – केवल; सिद्धिम् – सफलता; समधिगच्छति – प्राप्त करता है,
भावार्थ : मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता (जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम 'निष्कर्मता' है।) को यानी योगनिष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्यागमात्र से सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठा को ही प्राप्त होता है॥4॥
तात्पर्य : भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है । शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती । ज्ञानयोगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है । किन्तु भगवान् कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते । हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है । दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान् की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान् स्वीकार कर लेते हैं (बुद्धियोग) । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् । ऐसे सिद्धान्त की रंचमात्र सम्पन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है ।
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥५॥
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥५॥
न – नहीं; हि – निश्चय ही; कश्र्चित् – कोई; क्षणम् – क्षणमात्र; अपि – भी; जातु – किसी काल में; तिष्ठति – रहता है; अकर्म-कृत् – बिना कुछ किये; कार्यते – करने के लिए बाध्य होता है; हि – निश्चय ही; अवशः – विवश होकर; कर्म – कर्म; सर्वः – समस्त; प्रकृति-जैः – प्रकृति के गुणों से उत्पन्न; गुणैः – गुणों के द्वारा,
भावार्थ : निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है॥5॥
तात्पर्य : यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है । आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता । यह शरीर मृत-वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील (सक्रीय) रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता । अतः आत्मा को कृष्णभावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा । माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाय । किन्तु यदि आत्मा कृष्णभावनामृत के अपने स्वभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है । श्रीमद्भागवत (१.५.१७) द्वारा इसकी पुष्टि हुई है –
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्नपक्कोSथ पतेत्ततो यदि ।
यत्र क्क वाभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तोSभजतां स्वधर्मतः ।।
यत्र क्क वाभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तोSभजतां स्वधर्मतः ।।
यदि कोई कृष्णभावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाय तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी । किन्तु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्णभावनाभावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? अतः कृष्णभावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है । अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्णभावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है ।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥
कर्म-इन्द्रियाणि – पाँचो कर्मेन्द्रियों को; संयम्य – वश में करके; यः – जो; आस्ते – रहता है; मनसा – मन से; स्मरन् – सोचता हुआ; इन्द्रिय-अर्थान् – दम्भी; सः – वह; उच्यते – कहलाता है,
भावार्थ : जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है॥6॥
तात्पर्य : ऐसे अनेक मित्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्णभावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किन्तु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वात्सव में वे मन में इन्द्रियभोग का चिन्तन करते रहते हैं । ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किन्तु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं । इन्द्रियसुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है , किन्तु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधिविधानों के पालन में लिया जाय तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है । किन्तु जो अपने को योगी बताते हुए इन्द्रियतृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी-कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे । उसका ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे पजल भगवान् की माया द्वारा हर लिये जाते हैं । ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता ।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥
यः – जो; तु – लेकिन; इन्द्रियाणि – इन्द्रियों को; मनसा – मन के द्वारा; नियम्य – वश में करके; आरभते – प्रारम्भ करता है; अर्जुन – हे अर्जुन; कर्म-इन्द्रियैः – कर्मेन्द्रियों से; कर्म-योगम् – भक्ति; असक्तः – अनासक्त; सः – वह; विशिष्यते – श्रेष्ठ है,
भावार्थ : किन्तु हे अर्जुन! जो पुरुष मन से इन्द्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥7॥
तात्पर्य : लम्पट जीवन और इन्द्रियसुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रह कर जीवन-लक्ष्य को, जो भवबन्धन से मुक्त होकर भगवद्धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है । प्रमुख स्वार्थ-गति तो विष्णु के पास जाना है । सम्पूर्ण वर्णाश्रम-धर्म का उद्देश्य इसी जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति है । एक गृहस्थ भी कृष्णभावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुँच सकता है । आत्म-साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है । इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है । जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी (धूर्त) से कहीं श्रेष्ठ है और जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी अध्यात्मिकता का जमा धारण करता है । जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है ।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥८॥
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥८॥
नियतम् – नियत; कुरु – करो; कर्म – कर्तव्य; तवम् – तुम; कर्म – कर्म करना; ज्यायः – श्रेष्ठ; हि – निश्चय ही; अकर्मणः – काम न करने की अपेक्षा; शरीर – शरीर का; यात्रा – पालन, निर्वाह; अपि – भी; च – भी; ते – तुम्हारा; न – कभी नहीं; प्रसिद्धयेत् – सिद्ध होता; अकर्मणः – बिना काम के,
भावार्थ : तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा॥8॥
तात्पर्य : ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अपने आप को उच्चकुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े-बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है । श्रीकृष्ण यः नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे । अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे । ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है । देह-निर्वाह के लिए किये गए तथाकथित त्याग (संन्यास) का अनुमोदन न तो भगवान् करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही । आखिर देह-निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है । भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं । इस जगत् का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात् इन्द्रियतृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है । ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है । नियत कर्मों द्वारा ऐसा किये बिना मनुष्य की चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी (योगी) बनने तथा सारा काम छोड़ कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे ।


























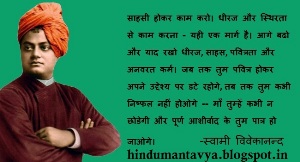





0 comments